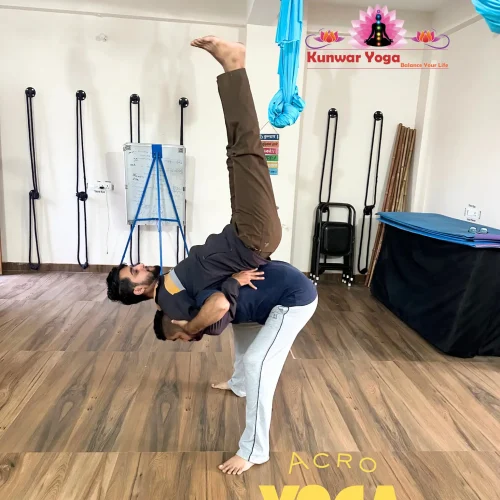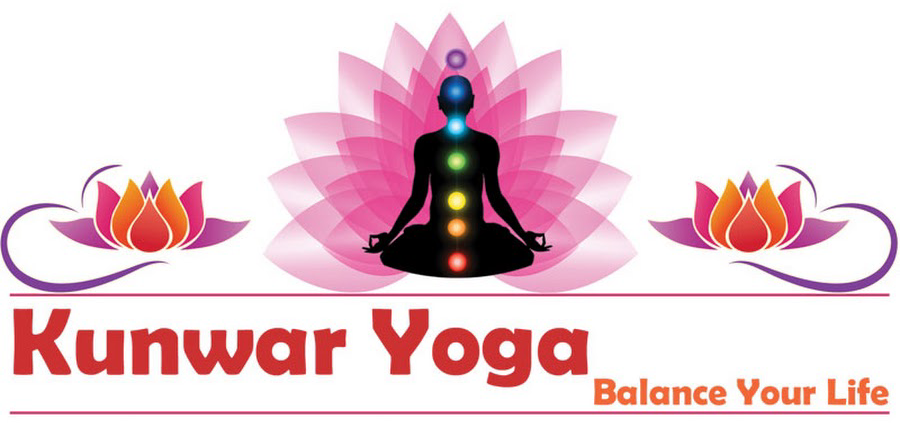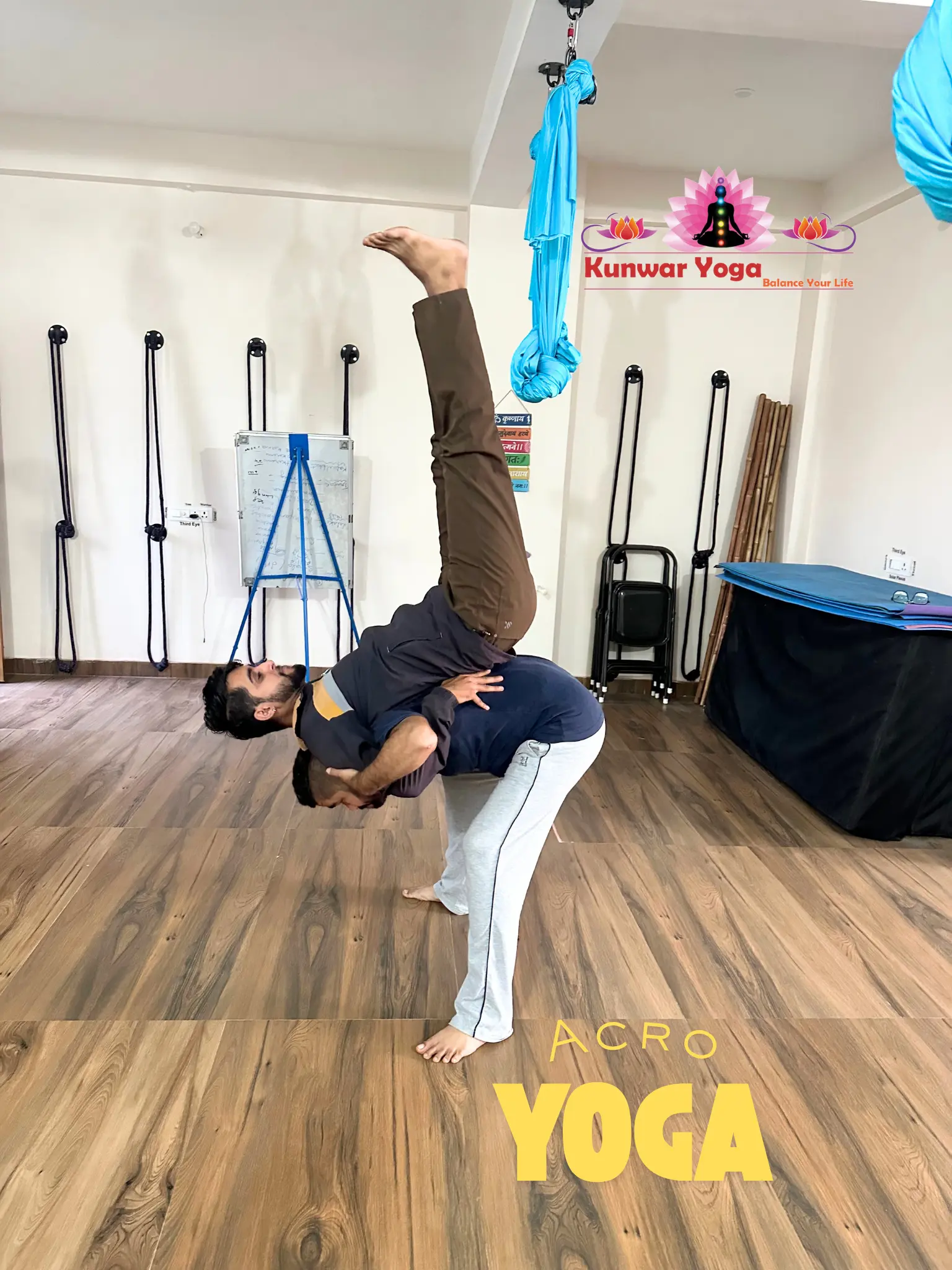Table of Contents
Toggleयोग अभ्यास के लिए सही स्थान (जगह), वातावरण और आहार (भोजन)
स्थान (जगह), वातावरण और आहार (भोजन) – योगाभ्यास में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कई बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे – उचित स्थान, समय, वातावरण, आहार आदि; क्योंकि इन सबका हमारे योगाभ्यास की सफलता में काफी योगदान है। विध्नरहित स्थान जैसे कोलाहल से दूर खुली हवा में योगाभ्यास करना काफी अच्छा हो सकता है। उचित समय एवं वातावरण का भी योगाभ्यास में काफी महत्त्वपूर्ण स्थान है। योगाभ्यास में आहार का महत्त्व तो विशेष रूप से है, क्योंकि उचित आहार-विहार ही हमारी योग साधना को उच्च श्खिर पर पहुँचा सकता है। कहा भी गया है –
जैसा खाए अन्न वैसा बने मन।
हमारे यौगिक ग्रंथों जैसे – हठ प्रदीपिका, घेरण्ड संहिता आदि में उपयुक्त स्थान, समय, वातावरण तथा आहार के बारे में काफी चर्चा की गई है। इन्हीं के आधार पर हम उपरोक्त विषयों की विस्तार से चर्चा करेंगे।
योगाभ्यास के लिए उचित स्थान (योगमठ) कैसा होना चाहिए इन हिंदी
योगाभ्यास के लिए उचित स्थान (योगमठ) – वह स्थान जहाँ साधक साधना प्रारंभ करता है उसे मठ कहते हैं। साधनात्मक जीवन में स्थान का विशेष महत्त्व है। प्राचीन भारतीय योग परंपरा में ऋषियों ने ऐसे स्थानों का चयन किया जहाँ उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव था।
इसलिए ऋषिगण पहले साधना के लिए हिमालय का चयन किया करते थे, क्योंकि वहाँ पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी अपितु ध्यान स्वत: ही लग जाता था। हमारे ऋषियों मुनियो ने उचित स्थान पर कठोर साधना करके सिद्धियों की प्राप्ति की आज आधुनिक नगरीय वातावरण में भी उचित खुला स्थान देखकर ही योगाभ्यास का प्रारंभ करना चाहिए।
वह नियम स्थान जहाँ पर मन की निम्नगामी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है वह स्थान योग मठ कहलाता है। योगमठ दो शब्दों, योग और मठ से मिलकर बना है।
योग – जीवन के उददेश्यों को पूर्ण करने के लिए संकल्पपूर्वक किया गया कार्य ही योग है।
मठ –जहाँ मन का ठहराव हो अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सके, उसे मठ कहते हैं।
इस प्रकार योगमठ वह स्थान है, जहाँ योग की साधना की जाती है। जो व्यक्ति समाज के कल्याण और विभिन्न आध्यात्मिक कार्यों के लिए संकल्प लेता है, उसे ऐसे स्थान को आवश्यकता होती है।
अर्थात वह स्थान है जो आध्यात्मिक शक्तियों से भरा हो, जहाँ योगी संत चित्त होकर योगाभ्यास कर सकें। वैसे स्थान को योगमठ कहते हैं। अत: योगाभ्यास के निमित्त सात्तिवक वातावरण होना आवश्यक है, ताकि साधक साधना कर अपने लक्ष्य को पा सके।
योगमठ कहाँ बनाएँ –
अब प्रश्न उठता है कि योगमठ कहाँ बनाया जाए। यह तो जाहिर – सी बात है कि जन कोलाहल से दूर एकांत तथा खुले वातावरण में योगमठ बनाना चाहिए। जहाँ लोग मन पर नियंत्रित करके शांति से योगाभ्यास कर सके। इस संबंध में घेरण्ड संहिता तथा हठप्रदीपिका में चर्चा की गयी हैं।
घेरण्ड संहिता के अनुसार –
सुदेशे धार्मिके राज्ये सुभिक्षे निरूपद्रवे।
कृत्वा तत्रैकं कुटीरं प्राचीरैः परिवेष्टितम् ॥ – घेरण्ड
ऐसा सुन्दर धार्मिक स्थान जहाँ भोजन के लिए खाद्य पदार्थ सहजता से उपलब्ध हो और वहाँ किसी प्रकार का उपद्रव न हो और कुटी के चारों तरफ चारदीवारी हो।
सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरूपट्रवे।
धनु: प्रमाणपर्यत शिलाग्नि जल वर्जित
एकांते मठिकामध्ये स्थातव्यं हठयोगिना ॥ – हठप्रदीपिका
सुराज्ये, धार्मिक तथा निरूपद्रव देशा में एक छोटी कुटीर बनाकर योगी को रहना चाहिए, जिसके चारों ओर चार हाथ की दूरी तक पत्थर, अग्नि अथवा जल न हो। ‘सुराज्ये’ से अभिप्राय है कि वह स्थान प्राकृतिक सुर्षमा तथा वन्य संपदाओं से परिपूर्ण हो।
धार्मिक देश’ से तात्पर्य है, वहाँ के निवासी धार्मिक प्रवृत्ति के हों। ‘सुभिक्षे’ से अभिप्राय है, अन्न, जल, फल, मूल आदि का अभाव न हो। ‘निरूपद्रवे ‘ का अभिप्राय है कि उस स्थान विशेष के समाज में नियम और व्यवस्था हो, किसी प्रकार की हिंसा की बात न हो। तात्पर्य यह है कि योग की सफलता के लिए साधकों में मानसिक शांति बनी रहे। इसलिए विघ्नरहित स्थान में अभ्यास करना चाहिए।
योगमठ किस जगह न बनाएं?
घेरण्ड संहिता के अनुसार –
दूरदेशे तथाअरण्ये राजधान्यां जनांतिके।
योगारंभं न कुर्वीत कृतश्चेत्सिद्धिहा भवेत् ॥ – घेरण्ड सहिता 5/3
दूर देश में (परदेश में), जंगल के बीच में, राजधानी में जहाँ लोगों का आना-जाना अधिक हो, ऐसे जगह पर योगाभ्यास करने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है।
अविश्वासं दूरदेशो अरण्ये रक्षिवर्जितम्।
लोकारण्ये प्रकाशश्च तस्मात्त्रीणि विवर्जयेत्। – घेरण्ड संहिता 5/4
क्योंकि परदेश में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जंगल में असुरक्षित रहेंगे और राजधानी में लोगों के अत्यधिक आने – जाने से प्रकाश और कोलाहल रहता है। अत: उपर्युक्त तीन स्थानों में योगाभ्यास करना वर्जित है। अत: योग साधना का अभ्यास दूए देश या दूर जंगल या राजधानी अर्थात जनता के बीच नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास के लिए पूर्णतः एकांत भी वर्जित है और भीड़ से भरा स्थान भी।
योगमठ कैसा चाहिए –
घेरण्ड संहिता तथा हठप्रदीपिका मे योगमठ के स्वरूप के संबंध में चर्चा की गई है।
वापी कूपतडागं च प्राचीर मध्यवर्त्ति च।
नात्युच्चं नातिनिम्नं च कुटीरं कीट वर्जितम्॥
साम्यग्गोमयलिप्तं च कुटीरं तत्र निर्मितम्।
एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायामं समभ्यसेत्॥ – घेरण्ड संहिता
योगमठ के आस – पास कुआँ और तालाब हो और योगमठ चारों तरफ से घिरा हुआ हो। कुटीरं की भूमि न ज्यादा ऊंची हो और न नीची हो। समतल हो और वहाँ कीड़े – मकोड़ न हों। वहाँ बिल या छिद्र आदि न हो। गाय के गोबर से लिपा होना चाहिए। ऐसे गुप्त स्थान में कटी बनाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए।
हठप्रदीपिका के अनुसार –
अल्पद्वारमरन्श्रगर्तविवर नात्युच्चनीचायतम्।
सम्यग्गोमयसान्द्रलिप्तममलं निःशेषजन्तूज्झितम।
बाहों मण्डपवेदिकूपरुचिर प्राकारसंवेष्टितम्।
प्रोक्तं योगमठस्य लक्षणमिंद सिद्धैर्हठाभ्यासिभि:॥ – हठप्रदीपिका ॥
योगमठ का दरवाजा न छोटा हो न बड़ा हो, वहाँ छिद्र न हो, बिल या सुरंग न हो, वहाँ की भूमि न ऊँची हो न नीची। समतल हो, गाय के शुद्ध गोबर से लिपी होनी चाहिए। कीडे – मकोड़े से रहित हो। जंगली जंतु से रहित हो। कुटीर के बाहर मंडप, वेदि यानि यज्ञशाला हो और बगल में कुआँ जिसमें स्वच्छ जल हो, वहाँ प्रकाश का आवागमन हो, वहाँ घेरा लगा दिया गया हो।
इस प्रकार उपर्युक्त लक्षणों से युक्त ‘योगमठ’ में योगाभ्यास करने से सिद्धि सुनिश्चित है। साधकों में मानसिक शांति बनी रहेगी। अत: योग में सफलता के लिए उपर्युक्त वर्णित विघ्नरहित स्थान ऐसे लोगों के लिए निषिद्ध नहीं है जिन्हें स्थान न मिलता हो। किंतु योगियों का इस प्रकार के स्थान में योगाभ्यास सफलता प्राप्त करना सुगम हो जाता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अपने घर को ही योगमठ बनाना चाहिए।
योगाभ्यास के लिए सही समय एवं वातावरण –
योग साधना में काल का महत्त्वपूर्ण स्थान है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए एक उपयुक्त समय होता है। उसी प्रकार योगाभ्यास प्रारंभ करने के लिए भी उचित समय का ज्ञान होना आवश्यक है। अनुकूल समय में कार्य करने से उनकी कार्य-शैली में वृद्धि होती है। अत: योग साधकों को अभ्यास आरंभ करने के लिए उपयुक्त समय का चयन करना चाहिए, जिससे सिद्धि की प्राप्ति हो सके।
प्रारंभिक साधकों को ऐसे समय का चुनाव करना चाहिए जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो सके, क्योंकि उचित समय पर अभ्यास करने से कोई भी कार्य उनके लिए अस्वाभाविक नहीं रह पाता है। उपयुक्त समय में की गई साधना या क्रिया-कलाप साधक के जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है।
अतः योगाभ्यासी को ऐसे समय का चुनाव करनी चाहिए, जिसमें अधिक गरमी, सरदी या बरसात न हो, अर्थात समशीतोष्ण मौसम का चयन करना चाहिए। जिस मौसम में वातावरण प्राणशक्ति से ओतप्रोत हो, वैसे समय में योगाभ्यास करना उचित एवं अधिक लाभप्रद होता है। हमारे ऋषि-मुनियों ने योगशास्त्र या प्रकृति के इन्हीं नियमों को जानकर-समझकर योगाभ्यास के लिए विशेष काल का निर्धारण किया है। आयुर्वेदशास्त्र, घेरण्ड संहिता तथा गीता में इसकी चर्चा मिलती है।
आयुर्वेदशास्त्र में महर्षि चरक ने कहा है –
कालो हि नाम भगवान् स्वयंभूरनादि मध्यनिघने॥
आचार्यों ने काल को ही स्वयंभू, अनादि, मध्यरहित एवं अनंत माना है। योगाभ्यास के लिए निषिद्ध समय – घेरण्ड संहिता के पाँचवे अध्याय के आठवे श्लोक में कहा गया है –
हेमंते शिशि रे ग्रीष्मे, वर्षयां च ऋतौ तथा।
योगारंभं न कुर्वीत, कृते योगो हिरोगद:॥ – 5/8
हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा में योगाभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। इन चार ऋतुओं में योगाभ्यास प्रारंभ करने से यह रोग प्रदायक हो जाता है।
योगाभ्यास के लिए उपयुक्त समय –
वंसते शरदि प्राक्त योगारंभ समाचरेत्।
तदा योगी भवेत्सिद्धो रोगान्मुक्तो भवेद् ध्रुवम्॥
बसंत और शरद ऋतु में योगाभ्यास शुरू करने से योग साधक निश्चित ही सिद्धि प्राप्त करता है और रोगों से मुक्त रहता है। जब वातावरण में प्राणवायु विद्यमान हो उस समय प्राणायाम का अभ्यास करता चाहिए। ऐसे समय को साधना के लिए उपुयक्त माना जाता है। बल के बिना व्यक्ति ज्ञाननहीं, प्राप्त कर सकता। यहाँ बल का तात्पर्य शक्ति से नहीं, बल्कि प्राण से है, अर्थात जिसके पास प्राण शक्ति अधिक रहेगी वही योगाभ्यास कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यदि साधक प्रतिकूल परिस्थितियों में योगाभ्यास करे तो इसका प्रतिकूल परिणाम साधक को भुगतना पड़ता है और यदि अनुकूल परिस्थितियों में योगाभ्यास किया जाए तो इसका अनुकूल परिणाम होगा।
इसे भी पढे – नाद योग का अर्थ, परिभाषा एवं नाद योग क्या है इन हिंदी