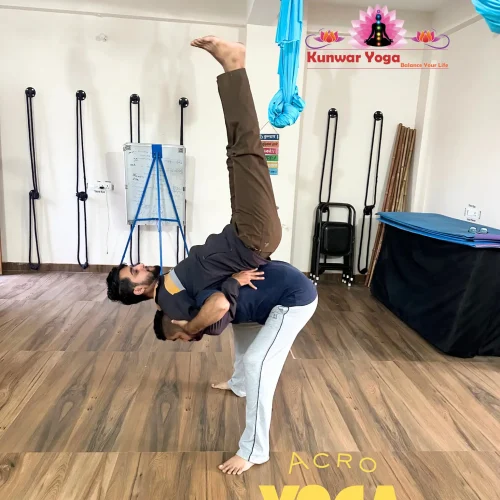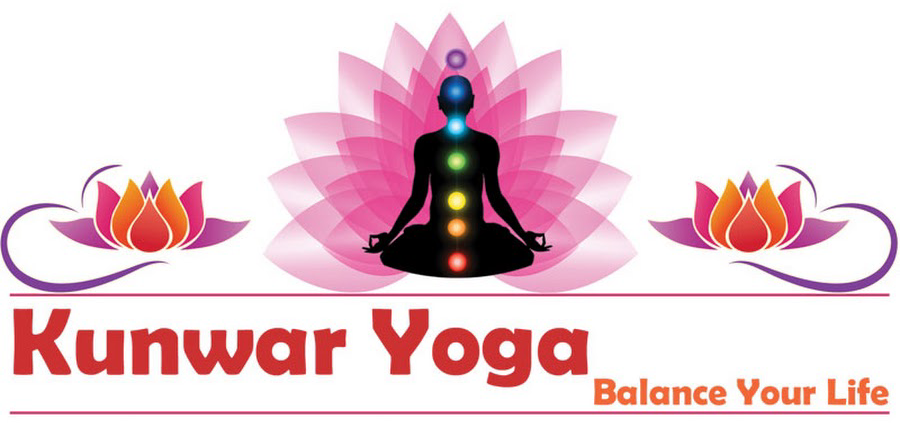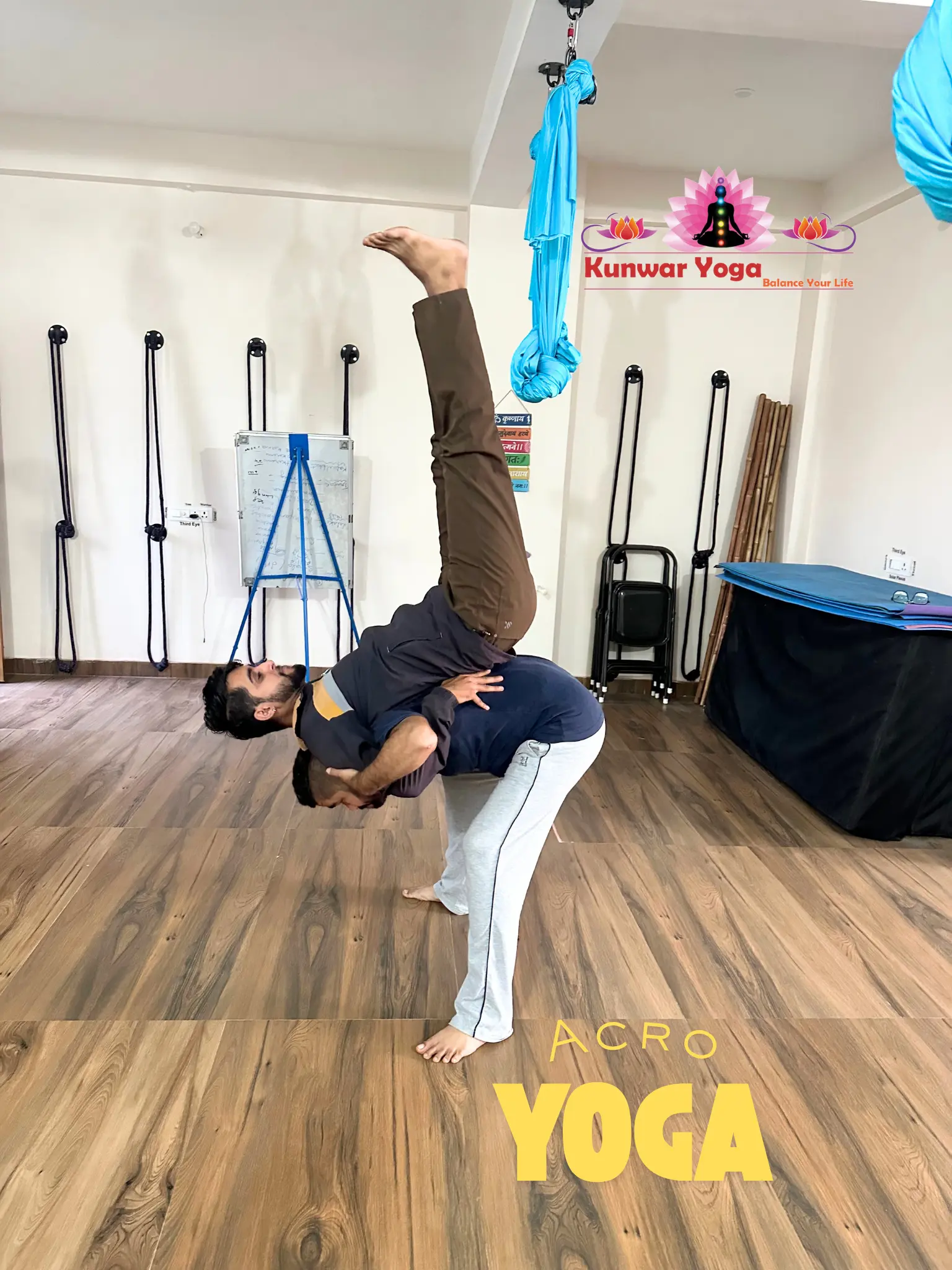Table of Contents
Toggleहठयोग –
योग विद्या के विविध आयामों में हठयोग (HathaYog) का अपरिहार्य स्थान है। कहा जाता है कि हठयोग (HathaYog) और तंत्र विद्या का संबंध अधिक निकट है अर्थात तंत्र विद्या से हठयोग (HathaYog) की उत्पत्ति हुई। ऐसा कथन इसलिए कहा गया होगा कि भगवान शिव इन दोनों (तंत्र और हठ विद्या) के आदि प्रणेता थे और उन्हीं से इन विद्याओं का आविर्भाव हुआ।
एक और मान्यता प्रचलित है कि चौदहवीं – पंद्रह्वी शताब्दी मैं तंत्र विद्या का विस्तार भारतवर्ष में चरमोत्कर्ष पर था। अधिक विस्तारित एवं प्रचलित होने के कारण इसका दुरुपयोग होने लगा। फलतः समाज में त्राहि- त्राहि मच गई। तब उसी काल में मत्स्येंद्रगाथ और गोरखनाथ जी ने इस विद्या के विकृत रूप को परिष्कृत कर उसे सर्वसुलभ हठयोग विद्या के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। जो राजयोग के एक अभिंन अंग के रूप में प्रचलित होती आ रही है।
हठयोग (HathaYog) का इतिहास | हठयोग का अर्थ एवं परिभाषा इन हिंदी
हठयोग की उत्पत्ति –
श्री आदिनाथाय नमोऽस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या।
विभ्राजते प्रोन्नतराजायोगमारोदुमिच्छोरधिरोहिणीव ।।
उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठयोग (HathaYog) विद्या की शिक्षा दी, जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर पहुँचने की इच्छा रखने वाले अभ्यासियों के लिए सीढ़ी के समान है।
ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने, जिन्हें यहाँ आदिनाथ कहा गया है, सर्वप्रथम अपनी पत्नी पार्वती को हठयोग की शिक्षा दी। हठयोग (HathaYog) एवं तंत्र संबंधी ग्रंथ शिव – पार्वती संवाद के रूप में हैं।
किन्तु भारतवर्ष इस अर्थ में सौभाग्यशाली रहा है कि जब- जब भी विकृतियाँ पैदा हुईं और अपनी चरम सीमा पर पहुँचती दिखाई दीं, तब – तब कोई न कोई महापुरुष उत्पन्न होते रहे, हमें निर्देश देते रहे और हमारा सही मार्गदर्शन करते रहे हैं।
ऐसे ही महापुरुष श्री मत्स्येन्द्रनाथ जी भी हुए जिन्होंने तंत्र विद्या के माध्यम से ही सर्वप्रथम हठयोग (HathaYog) की विद्या जन – जन तक पहुँचाई। इनके पश्चात गोरक्षनाथ, स्वात्माराम जी ने इन्हें आगे विस्तारित करने में संपूर्ण सहयोग प्रदान किया स्वात्माराम जी के अनुसार श्री आदिनाथ (( भगवान शिव) ही हठयोग परंपरा के आदि आचार्य हैं।
हठयोग का अर्थ एवं परिभाषा –
‘ह’ और ‘ठ’ दो भिन्न वर्ण के मिलन से हठ शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ‘ह’ का अर्थ सूर्य और ‘ठ’ चंद्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये सूर्य और चंद्र मनुष्य शरीर में विद्यमान नाड़ियों के नाम बताने के अर्थ में प्रयुक्त हैं, जिसे पिंगला या इडा भी कहा जाता है। अन्यान्य दो विपरीतधर्मी तत्व के संकेत के रूप में भी ‘ह’ और ‘ठ का प्रयोग मिलता है जैसे – प्राण और अपान, पित्त और कफ़, ग्रीष्म और शीत, दिन आर रात, शिव और शक्ति आदि।
हकारः कथितः सूर्य ठकारचन्द्र उच्यते।
सूर्य चन्द्रमसोर्योगात् हठयोग निगधते ।।
हकार सूर्य स्वर और ठकार से चंद्र चलते हैं। इन सूर्य और चंद्र स्वर को प्राणायाम आदि का विशेष अभ्यास कर प्राण की गति को सुषुम्नावाहिनी कर लेना ही हठयोग (HathaYog) है।
मनुष्य शरीर में अवस्थित नाड़ियों से प्राणतत्त्व का संवाहन होता है, उनमें मुख्यतः सूर्य और चंद्र दो नाड़ी प्रधान हैं। इन दोनों के बीच में और एक शक्ति संपन्न नाड़ी है, सुषुम्ना। दो भिन्न नाड़ियों में प्रवाहित होने वाले प्राण को एक धारा में समाहित कर उसे सुषुम्नागामी बनाने की प्रक्रिया को हठयोग (HathaYog) कहते हैं। प्राणायाम आदि क्रिया के माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न होती है।
इस प्रकार विखंडित प्राण प्रवाह को संवाही किया जाता है तब उस में अधिक शक्ति और गति पैदा होती है। फलस्वरूप प्राण का गुण ऊर्ध्वगामी होता है। शरीर में स्थित विभिन्न चक्र होते हुए प्राण का एक निर्दिष्ट मार्ग होता है। उर्ध्व मार्ग में आने वाले चक्र क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा को भेदन करते हुए सहस्त्रार की ओर गमन करता है। अंत में जब सहस्त्रार तक पहुँचता है तो यह अवस्था एक सिद्ध अवस्था कहलाती है।
सुषुम्ना वाही प्राण की यह चरर्मोत्कर्ष अवस्था है। यही योग का चरम उत्कर्ष है। इसी अवस्था को समाधि, आत्मदर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार आदि नाम भी दिया जाता है। यह एक हठयोगी के लिए अभीष्ट लक्ष्य होता है। शिव् शव रशक्तिका मिलन इसी बिंदु पर होता है।
शिव जो समष्टि अर्थात परमात्मा तत्त्व के रूप में है और शक्ति जो व्यष्टि अर्थात जीवात्मा के अस्तित्व के रूप में है। इस प्रकार आत्मा का परमात्मा में और शिव का शक्ति में एकाकार या समरूप होना ही योग है। इसी को प्राप्त करने का सर्वसिद्ध माध्यम हठयोग (HathaYog) है। चित्तवृत्ति निरोध द्वारा आत्मा की प्राप्ति के लिए करने योग्य द्वितीय श्रेणी को क्रियाओं का नाम हठयोग है। योग का अर्थ इन दोनों का संयोजन या एकीकरण है।
योग शब्द कई अर्थों में लिया जाता है – जैसे गणित शास्त्र में दो या दो से अधिक अंकों के मेल को योग कहा जाता है, आयुर्वेद में दो या अधिक औषधियों का मेल योग है, आध्यात्मिक भाषा में आत्मा और परमात्मा का मिलन योग होता है। इसी प्रकार यहाँ सूर्य एवं चंद्र के एकीकरण या संयोजन को एक माध्यम हठयोग (HathaYog) है।
मनुष्य के अंदर दो प्रमुख शक्तियां सदैव ही कार्यरत रहती हैं वे हैं – (1) मन और ( 2) प्राण। मानसिक प्रक्रिया के कारण मनुष्य को ”धन’ (+) तथा प्रकृति को ऋण (- ) माना गया है, जिसके प्रतीक सूर्य एवं चंद्र हैं। सूर्य का स्थान मनुष्य के शरीर में दाया तथा चंद्र का बायाँ है। हठ शब्द’ ह, क्ष’ का विकृत रूप है। इन अक्षरों का अर्थ है- ह = सूर्य शक्ति का प्रतीक है। क्ष = चंद्र शक्ति का प्रतीक है।
दूसरे मतानुसार हठयोग का अर्थ होता है- हकार और ठकार का योग | हठयोग (HathaYog) का संबंध शरीर से एवं श्वास नियंत्रण से है। ‘ह’ एवं ‘ठ’ को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है – ह = सूर्य, पिंगला, ग्रीष्म, पित्त, शिव, दिन एवं रजस | ठ = चंद्र, इड़ा, शीत, कफ, शक्ति, रात एवं तमस। सूर्य और चंद्र शब्दों की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है।
एक व्याख्या के अनुसार सूर्य से तात्पर्य प्राणवायु तथा चंद्र का अपान वायु है। अतः प्राणायाम के अभ्यास द्वारा उक्त दोनों प्रकार की वायु का निरोध हठयोग है। इस प्रकार हठयोग (HathaYog) वह क्रिया है जिसमें इड़ा और पिंगला नाड़ी के सहारे प्राण को सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से षट्चक्रों का क्रमशः भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र में ले जाकर समाधिस्थ कर दिया जाता है।
योगशिखोपनिषद् में योग को परिभाषा करते हुए कहा गया है कि अपान व प्राण, रज व रेतस् सूर्य व चंद्र तथा जीवात्मा व परमात्मा का मिलन योग है। यह परिभाषा भी हठयोग की सूर्य व चंद्र के मिलन की स्थिति को प्रकट करती हैं।
ह (सूर्य) का अर्थ सूर्य स्वर, दायाँ स्वर, पिंगला स्वर अथवा यमुना तथा ठ (चंद्र) का अर्थ चंद्र स्वर, बायाँ स्वर, इड़ा स्वर अथवा गंगा लिया जाता है। दोनों के संयोग से अग्निस्वर, मंध्य स्वर, सुषुम्ना स्वर अथवा सरस्वती स्वर चलता है, जिसके कारण ब्रह्मनाड़ी में प्राण का संचरण होने लगता है। इसी ब्रह्मनाड़ी के निचले सिरे के पास कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था में स्थित है।
जब साधक प्राणायाम करता है तो प्राण के आघात से सुप्त कुंडलिनी जाग्रत होती है तथा ब्रह्मनाड़ी में गमन कर जाती है जिससे साधक में अनेकानेक विश्ष्टिताएँ आ जाती हैं। यह प्रक्रिया इस योग पद्धति में मुख्य है। इसलिए इसे हठयोग (HathaYog) कहा गया है।
यही पद्धति आज आसन, प्राणायाम, षट्कर्म, मुद्रा आदि के अभ्यास के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय हो रही है। महर्षि पतंजलि ने मनोनिग्रह के साधन रूप में इस पद्धति का प्रयोग उपयोगी बताया है।
हठयोग (HathaYog) के फायदे
हठयोग करने से शरीर को अनगिनत फायदे मिल सकते हैं. हठयोग शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है. इसके नियमित अभ्यास से शक्ति, लचीलापन और संतुलन बढ़ता है. साथ ही तन और मन को शांति मिलती है. हठयोग करने से मिलने वाले फायदे इस प्रकार हैं –
इम्यून सिस्टम बेहतर करे
स्वस्थ रहने के लिए इम्यून सिस्टम का बेहतर होना जरूरी होता है. हठयोग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है. इसलिए, यह योग नियमित रूप से जरूर करना चाहिए.
कमर दर्द कम करे
बढ़ती उम्र में अधिकतर लोगों को कमर दर्द का सामना करना पड़ता है. गलत पोश्चर में बैठना व इनएक्टिव लाइफस्टाइल कमर में दर्द के मुख्य कारण माने जाते हैं. हठयोग (HathaYog) के अभ्यास से कमर के दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है. दरअसल, एक अध्ययन से पता चला है कि लगातार 21 दिन तक हठयोग करने से कोर मसल्स को ताकत मिलती है. साथ ही इससे शरीर के संतुलन में भी सुधार होता है. इसे रोजाना करने से कमर दर्द में आराम मिल सकता है.
तनाव से राहत
जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च में छपे 2013 के एक अध्ययन में पाया गया कि नियमित रूप से हठयोग करने से तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है. रोजाना 90 मिनट तक इस योग का अभ्यास करने से स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है.
इतना ही नहीं 2018 में हुए एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि अगर नियमित रूप से हठयोग के 12 सेशन किए जाएं, तो इससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन को दूर करने में मदद मिल सकती है.
हृदय बनाए स्वस्थ
अगर हृदय को हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हठयोग को जीवनशैली में जरूर शामिल करें. इस योग का अभ्यास करने से हृदय में रक्त का प्रवाह बेहतर रहता है. हृदय पूरे शरीर में ब्लड को सही तरीके से पंप कर पाता है. नियमित रूप से हठयोग करने से हृदय से जुड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है.
मजबूत हड्डियां
हठयोग (HathaYog) का नियमित अभ्यास करने से हड्डियां भी मजबूत बनती हैं. जर्नल ऑफ फिजिकल थेरेपी साइंस में 2015 के एक अध्ययन से पता चलता है कि हठयोग करने से रीढ़ और हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होता है. शोधकर्ता उन बुजुर्गों को हठयोग करने की सलाह देते हैं, जो अक्सर जोड़ों में दर्द से परेशान रहते हैं या जिन्हें हड्डियों को मजबूत बनाने की जरूरत है.
दमकती त्वचा
हठयोग (HathaYog) त्वचा को भी खूबसूरत बनाने में मदद कर सकता है. दरअसल, हठयोग करने से शरीर में ब्लड फ्लो सही रहता है. वहीं, इस योग को करने से तनाव और चिंता भी दूर होती है. सही ब्लड फ्लो और स्ट्रेस फ्री रहने से त्वचा में निखार आता है. त्वचा में प्राकृतिक चमक बनी रहती है.
हठयोग (HathaYog) में किए जाने वाले आसन
गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्मारात ने हठयोग प्रदीपिका को लिखा था. इसमें हठयोग को चार भागों में बांटा गया है – आसन, प्राणायाम, मुद्रा व समाधि. आसन के तहत 15 योगासनों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं –
- स्वस्तिकासन
- गोमुखासन
- वीरासन
- कुर्मासन
- कुक्कुटासन
- उत्तानकूर्मासन
- धनुरासन
- मत्स्येन्द्रासन
- पश्चिमोत्तासन
- मयूरासन
- शवासन
- सिद्धासन
- पद्मासन
- सिंहासन
- भद्रासन
इसी तरह प्राणायाम के तहत सूर्यभेदन, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भ्रस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्च्छा तथा प्लाविनी शामिल है. वहीं, मुद्रा में महामुद्रा, महाबंध, महावेध, खेचरी, उड्डीयान बन्ध, मूलबन्ध, जालंधर बन्ध, विपरीत करणी, वज्रोली, सहजोली, अमरोली, शक्ति चालान शामिल है.