Mr. Ajitesh Kunwar Founder of Kunwar Yoga – he is registered RYT-500 Hour and E-RYT-200 Hour Yoga Teacher in Yoga Alliance USA. He have Completed also Yoga Diploma in Rishikesh, India.


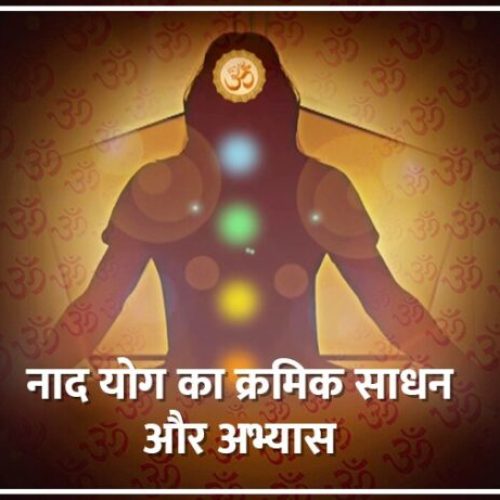
Kunwar Yoga – Mahadev Kunj, Old Nehru Colony, Dharampur, Dehradun, Uttarakhand, India. 248001


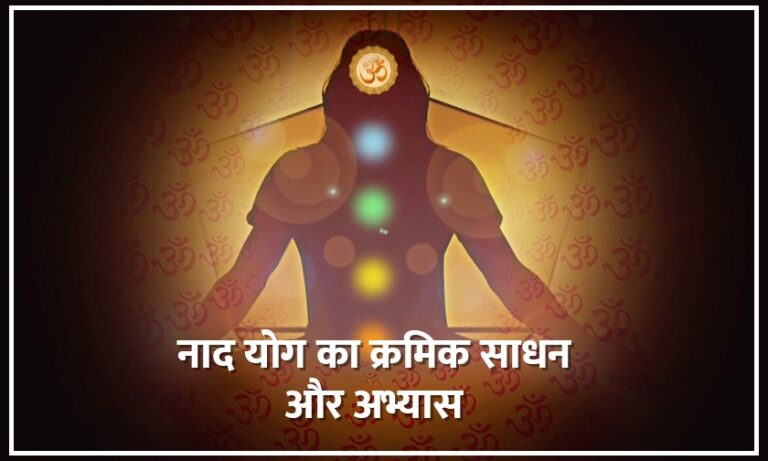
Copyright © 2024 Kunwar Yoga. | Design By : Website Designing Company Dehradun